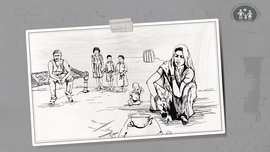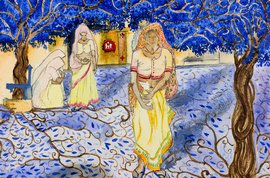आरिफ़ा, 82 साल की उम्र में सब कुछ देख चुकी हैं. उनका आधार कार्ड बताता है कि वह 1 जनवरी, 1938 को पैदा हुई थीं. आरिफ़ा को नहीं पता कि यह सही है या ग़लत, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर याद है कि 16 साल की उम्र में वह 20 साल के रिज़वान ख़ान की दूसरी पत्नी बनकर हरियाणा के नूह ज़िले के बिवान गांव आई थीं. आरिफ़ा (बदला हुआ नाम) याद करते हुए बताती हैं, “मेरी मां ने रिज़वान के साथ मेरी शादी तब कर दी थी, जब मेरी बड़ी बहन [रिज़वान की पहली पत्नी] और उनके छह बच्चों की मौत विभाजन के दौरान भगदड़ में कुचल जाने की वजह से हो गई थी."
उन्हें थोड़ा-थोड़ा यह भी याद है कि जब महात्मा गांधी मेवात के एक गांव में आए थे और मेओ मुसलमानों से कहा था कि वे पाकिस्तान न जाएं. हरियाणा के मेओ मुसलमान हर साल 19 दिसंबर को नूह के घासेड़ा गांव में गांधी जी की उस यात्रा की याद में मेवात दिवस मनाते हैं (2006 तक नूह को मेवात कहा जाता था).
आरिफ़ा को वह दृश्य आज भी याद है, जब मां ने उनको ज़मीन पर बैठाते हुए समझाया था कि उन्हें रिज़वान से क्यों शादी कर लेनी चाहिए. यह बताते हुए कि कैसे बिवान उनका घर बन गया, जोकि उनके गांव रेठोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है, आरिफ़ा कहती हैं, “उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, मेरी मां ने मुझसे कहा था. मेरी मां ने मुझे उसे दे दिया फिर.” दोनों ही गांव उस ज़िले का हिस्सा हैं जोकि देश के सबसे कम विकसित जिलों में से एक है.
राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दूर, फ़िरोज़पुर झिरका ब्लॉक का बिवान गांव, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर और अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है. दिल्ली से नूह को जाने वाली सड़क दक्षिणी हरियाणा के गुरुग्राम से होकर गुज़रती है, जो भारत में तीसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला एक वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है, लेकिन यहीं पर देश का सबसे पिछड़ा 44वां ज़िला भी है. यहां के हरे-भरे खेत, शुष्क पहाड़ियां, ख़राब बुनियादी ढांचे, और पानी की कमी आरिफ़ा जैसे कई लोगों के जीवन का हिस्सा हैं.
मेओ मुस्लिम समुदाय हरियाणा के इस क्षेत्र और पड़ोसी राज्य राजस्थान के कुछ हिस्सों में रहते हैं. नूह ज़िले में मुसलमानों की जनसंख्या की हिस्सेदारी 79.2 प्रतिशत है ( जनगणना 2011 ).
1970 के दशक में, जब आरिफ़ा के पति रिज़वान ने बिवान से पैदल दूरी पर स्थित रेत, पत्थर, और सिलिका की खदानों में काम करना शुरू किया, तब आरिफ़ा की दुनिया पहाड़ियों से घिर गई थी, और उनका प्रमुख काम पानी लाना था. बाईस साल पहले रिज़वान के निधन के बाद, आरिफ़ा अपना और अपने आठ बच्चों का पेट पालने के लिए खेतों में मज़दूरी करने लगीं, और तब उन्हें दिन भर की मज़दूरी मात्र 10 से 20 रुपए मिलती थी. वह बताती हैं, “हमारे लोग कहते हैं कि जितने बच्चे पैदा कर सकते हो करो, अल्लाह उनका इंतज़ाम करेगा."


आरिफ़ा: ‘गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करना अपराध माना जाता है' ; जब हम उनसे मिले थे, उनके हाथ में मोच थी. दाएं: बिवान में एक कमरे का घर , जिसमें वह अकेली रहती हैं
उनकी चारों बेटियां शादीशुदा हैं और अलग-अलग गांवों में रहती हैं. उनके चारों बेटे अपने परिवारों के साथ पास ही में रहते हैं; उनमें से तीन किसान हैं, एक निजी फ़र्म में काम करता है. आरिफा अपने एक कमरे के घर में अकेले रहना पसंद करती हैं. उनके सबसे बड़े बेटे के 12 बच्चे हैं. आरिफ़ा बताती हैं कि उनकी तरह ही उनकी कोई भी बहू किसी भी तरह के गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं करती. वह बताती हैं, “लगभग 12 बच्चों के बाद यह सिलसिला अपने आप रुक जाता है.” वह आगे जोड़ती हैं कि “गर्भनिरोधक का उपयोग करना हमारे धर्म में अपराध माना जाता है.”
रिज़वान की मृत्यु वैसे तो वृद्धावस्था में हुई थी, लेकिन मेवात ज़िले में अधिकतर महिलाओं ने तपेदिक (टीबी) के कारण अपने पतियों को खो दिया. टीबी के कारण बिवान में भी 957 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. उन्हीं में से एक बहार के पति दानिश (बदला हुआ नाम) भी थे. बिवान स्थित घर में वह 40 से अधिक वर्षों से रह रही हैं. उन्होंने 2014 से ही तपेदिक के कारण अपने पति के स्वास्थ्य को बिगड़ते देखा था. वह याद करती हैं, “उन्हें सीने में दर्द था और अक्सर खांसते समय ख़ून निकलता था." बहार, जो अब लगभग 60 साल की हैं, और उनकी दो बहनें, जो बग़ल वाले मकान में रहती हैं, उन सभी ने उस साल अपने पतियों को टीबी के कारण खो दिया था. “लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यही हमारी नियति थी. लेकिन हम इसके लिए पहाड़ियों को दोषी मानते हैं. इन पहाड़ियों ने हमें बर्बाद कर दिया है.”
(2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद और पड़ोसी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बाद हरियाणा में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध वाला आदेश केवल पर्यावरणीय क्षति के लिए है. इसमें टीबी का कोई उल्लेख नहीं है. केवल वास्तविक मामलों के विवरण और कुछ रिपोर्ट दोनों चीज़ों को जोड़ती हैं.)
यहां से सात किलोमीटर दूर, नूह के ज़िला मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), जोकि बिवान से सबसे नज़दीक है, वहां के कर्मचारी पवन कुमार हमें 2019 में तपेदिक के कारण हुई 45 वर्षीय वाइज़ की मृत्यु का रिकॉर्ड दिखाते हैं. रिकॉर्ड के अनुसार, बिवान में सात अन्य पुरुष भी टीबी से पीड़ित हैं. कुमार बताते हैं, “और भी कई मामले हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पीएचसी में नहीं आते."
वाइज़ की शादी 40 वर्षीय फ़ाइज़ा से हुई थी (दोनों के नाम बदल दिए गए हैं). वह हमें राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित अपने गांव के बारे में बताते हुए कहती हैं, “नौगांवा में कोई काम उपलब्ध नहीं था. मेरे पति को जब खानों में उपलब्ध काम के बारे में पता चला, तो वह बिवान चले आए. मैं एक साल बाद उनके पास गई, और हम दोनों ने यहां अपना एक घर बनाया.” फ़ाइज़ा ने 12 बच्चों को जन्म दिया. चार की मौत समय से पहले जन्म लेने के कारण हो गई. वह बताती हैं, “एक ठीक से बैठना भी नहीं सीख पाता था कि दूसरा बच्चा हो जाता था."
वह और आरिफ़ा अब 1,800 रुपए मासिक के विधवा पेंशन पर गुज़ारा कर रहे हैं. उन्हें काम शायद ही कभी मिल पाता है. 66 वर्षीय विधवा हादिया (बदला हुआ नाम) बताती हैं, “अगर हम काम मांगते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं. वे कहेंगे कि यह 40 किलो का है, कैसे उठाएगी ये?” वह उस ताने की नक़ल करते हुए यह बात कहती हैं जो उन्हें अक्सर सुनने को मिलते हैं. इसलिए, पेंशन का हर एक रुपया बचाया जाता है. चिकित्सा की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी नूह के पीएचसी तक जाने में ऑटोरिक्शा का 10 रुपए किराया देना पड़ता है, लेकिन ये लोग पैदल ही आते-जाते हैं और इस तरह से 10 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं. हादिया बताती हैं, “हम उन सभी बूढ़ी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं जो डॉक्टर के पास जाना चाहती हैं. फिर हम सभी वहां साथ जाते हैं. हम रास्ते में कई बार बैठते हैं, ताकि आराम करने के बाद आगे का सफ़र जारी रख सकें. पूरा दिन इसी में चला जाता है."
![Bahar (left): 'People say it happened because it was our destiny. But we blame the hills'. Faaiza (right) 'One [child] barely learnt to sit, and I had another'](/media/images/03a-IMG_1675-AB.max-1400x1120.jpg)
![Bahar (left): 'People say it happened because it was our destiny. But we blame the hills'. Faaiza (right) 'One [child] barely learnt to sit, and I had another'](/media/images/03b-IMG_1676-AB.max-1400x1120.jpg)
बहार (बाएं): ‘ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यही हमारी नियति थी. लेकिन हम पहाड़ियों को दोषी मानते हैं. ’ फ़ाइज़ा (दाएं): ‘ एक [बच्चा] मुश्किल से बैठना सीख पाता था कि दूसरा हो जाता था ’
बचपन में, हादिया कभी स्कूल नहीं गईं. वह बताती हैं कि हरियाणा के सोनीपत ज़िले के खेतों ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया, जहां उनकी मां मज़दूरी करती थीं. उनकी शादी 15 साल की उम्र में फ़ाहिद से हुई थी. फ़ाहिद ने जब अरावली की पहाड़ियों के खदानों में काम करना शुरू किया, तो हादिया की सास ने उन्हें खेतों में निराई करने के लिए एक खुरपा थमा दिया.
फ़ाहिद का जब 2005 में तपेदिक के कारण निधन हो गया, तो हादिया का जीवन खेतों में मज़दूरी करने, पैसे उधार लेने, और उसे चुकाने में बीतने लगा. वह आगे कहती हैं, “मैं दिन में खेतों पर काम करती और रात में बच्चों की देखभाल करती थी. फ़क़ीरनी जैसी हालत हो गई थी."
अपने ज़माने के प्रजनन संबंधी मुद्दों पर ख़ामोशी और प्रजनन संबंधी हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता की कमी का ज़िक्र करते हुए, चार बेटों और चार बेटियों की मां, हादिया कहती हैं, “मैंने शादी के पहले साल में एक बेटी को जन्म दिया. बाक़ी का जन्म हर दूसरे या तीसरे साल में हुआ. पहले का शुद्ध ज़माना था."
नूह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, गोविंद शरण भी उन दिनों को याद करते हैं. तीस साल पहले, जब उन्होंने सीएचसी में काम करना शुरू किया था, तो लोग परिवार नियोजन से जुड़ी किसी भी चीज़ पर चर्चा करने से हिचकिचाते थे. अब ऐसा नहीं है. शरण कहते हैं, “पहले, अगर हम परिवार नियोजन पर चर्चा करते, तो लोगों को गुस्सा आ जाता था. मेओ समुदाय में अब कॉपर-टी का उपयोग करने का निर्णय ज़्यादातर पति-पत्नी द्वारा लिया जाता है. लेकिन, वे अभी भी इसे परिवार के बुज़ुर्गों से छिपाकर रखना पसंद करते हैं. अक्सर महिलाएं हमसे अनुरोध करती हैं कि हम उनकी सास के सामने इसका खुलासा ना करें."
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (2015-16) के अनुसार, वर्तमान में नूह ज़िले (देहात) की 15-49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से केवल 13.5 प्रतिशत महिलाएं ही किसी भी प्रकार की परिवार नियोजन पद्धति का उपयोग करती हैं. हरियाणा राज्य के 2.1 की तुलना में नूह ज़िले में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 4.9 है (जनगणना 2011), जोकि बहुत ज़्यादा है. नूह ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में, 15-49 वर्ष की आयु की केवल 33.6 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं, 20-24 वर्ष की आयु की लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले ही कर दी जाती है, और केवल 36.7 प्रतिशत की डिलीवरी अस्पतालों में हुई है.
नूह ज़िले के ग्रामीण इलाक़ों में लगभग 1.2 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कॉपर-टी जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है. इसका कारण यह है कि कॉपर-टी को शरीर में एक बाहरी वस्तु के रूप में देखा जाता है. नूह पीएचसी की सहायक नर्स सेविका (एएनएम) सुनीता देवी कहती हैं, “किसी के शरीर में ऐसी कोई वस्तु डालना उनके धर्म के ख़िलाफ़ है, वे अक्सर कहती हैं.”


हादिया (बाएं) अपने एक कमरे के घर में: ‘हम उन सभी बूढ़ी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं जो डॉक्टर के पास जाना चाहती हैं. फिर हम लोग एक साथ वहां जाते हैं.' बिवान से सात किलोमीटर दूर स्थित नूह का पीएचसी (दाएं)
फिर भी, जैसा कि एनएफ़एचएस-4 से पता चलता है, परिवार नियोजन की ज़रूरतों का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है; अर्थात, महिलाएं गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन जो औरतें अगले जन्म को स्थगित (दो बच्चों में अंतर रखना) या बच्चे के जन्म को रोकना (सीमित करना) चाहती हैं – उनकी संख्या काफ़ी है, 29.4 प्रतिशत (ग्रामीण इलाक़ों में).
हरियाणा की चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) डॉ. रूचि (वह केवल पहले नाम का उपयोग करती हैं) कहती हैं, “चूंकि नूह में मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी है, “सामाजिक-आर्थिक कारणों से परिवार नियोजन के तरीक़ों के प्रति लोगों का झुकाव हमेशा कम रहा है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है. सांस्कृतिक कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं. वे हमसे कहती हैं, बच्चे तो अल्लाह की देन हैं. पत्नी नियमित रूप से गोली तभी खाती है, जब पति उसका सहयोग करता है और उसके लिए बाहर से ख़रीद कर लाता है. कॉपर-टी के साथ कुछ भ्रांतियां जुड़ी हैं. हालांकि, इंजेक्शन वाले गर्भनिरोधक, अंतरा को शुरू करने के बाद स्थिति में सुधार हो रहा है. इस विशेष विधि को लेकर पुरुष कोई हस्तक्षेप नहीं करते. कोई भी महिला अस्पताल जाकर इसकी ख़ुराक ले सकती है.”
इंजेक्शन द्वारा लिए जाने वाले गर्भनिरोधक ' अंतरा ' की एक ख़ुराक तीन महीने तक सुरक्षा प्रदान करती है और इसे हरियाणा में लोकप्रियता हासिल है, जोकि साल 2017 में इंजेक्शन वाले गर्भनिरोधकों को अपनाने वाला पहला राज्य था. जैसा कि एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है, तबसे 16,000 से अधिक महिलाओं ने इसका उपयोग किया है, जोकि विभाग द्वारा 2018-19 में निर्धारित किए गए 18,000 के लक्ष्य का 92.3 प्रतिशत है.
इंजेक्शन वाला गर्भनिरोधक जहां धार्मिक रुकावट की चिंताओं को दूर करने में मदद करता है, वहीं कुछ ऐसे अन्य कारक भी हैं जो परिवार नियोजन की सेवाएं पहुंचाने को बाधित करते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों में. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का उदासीन रवैया और स्वास्थ्य केंद्रों पर लंबे समय तक इंतज़ार करना भी महिलाओं को गर्भनिरोधक के बारे में सक्रिय रूप से सलाह लेने से रोकता है.
सीईएचएटी ( सेंटर फ़ॉर इंक्वायरी इन हेल्थ एंड अलाइड थीम्स , मुंबई में स्थित) द्वारा 2013 में यह पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराया गया कि स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न समुदायों की महिलाओं के बारे में धारणाओं पर आधारित धार्मिक भेदभाव की हक़ीक़त क्या है; तो पता चला कि वर्ग के आधार पर सभी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था; लेकिन, मुस्लिम महिलाओं ने ज़्यादातर परिवार नियोजन के अपने चुनाव, समुदाय के बारे में नकारात्मक टिप्पणी, और लेबर रूम में नीचा दिखाने वाले व्यवहार के रूप में इसका अनुभव किया.


नूह ज़िले का बिवान गांव (बाएं): नूह में कुल प्रजनन दर (टीएफ़आर) 4.9 है , जोकि काफ़ी ज़्यादा है. बिवान के अधिकांश पुरुषों ने अरावली की पहाड़ियों (दाएं) की खानों में काम किया है
सीईएचएटी की समन्वयक, संगीता रेगे कहती हैं, “चिंता का विषय यह है कि सरकार भले ही गर्भनिरोधकों के लिए अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न तरीक़े प्रदान करने का दावा करती हो; अक्सर यह देखा गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले प्रदाता ही सामान्य रूप से सभी महिलाओं के लिए इस प्रकार के निर्णय लेते हैं; मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें समझने और उनके साथ गर्भनिरोधक के सही विकल्पों पर चर्चा करने की ज़रूरत है.”
नूह में परिवार नियोजन की भारी ज़रूरत होने के बावजूद, एनएफ़एचएस-4 (2015-16) बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भनिरोधक का उपयोग करने वाली महिलाओं में से केवल 7.3 प्रतिशत ने ही कभी परिवार नियोजन पर चर्चा करने के लिए किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क किया था.
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), 28 वर्षीय सुमन, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से बिवान में काम किया है, का कहना है कि वह अक्सर महिलाओं पर ही छोड़ देती हैं कि वे परिवार नियोजन के बारे में अपना मन बनाएं और जब किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, तो अपने फ़ैसले के बारे में उनको बता दें. सुमन का कहना है कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की जर्जर हालत ही स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में बहुत बड़ी बाधा है. यह सभी महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित करता है, लेकिन बुज़ुर्ग महिलाओं को सबसे ज़्यादा.
सुमन कहती हैं, “नूह के पीएचसी तक जाने के लिए, हमें तिपहिया वाहन पकड़ने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है. केवल परिवार नियोजन की ही बात नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए, किसी को तैयार करने में मुश्किल होती है. पैदल चलने में वे थक जाती हैं. मैं वास्तव में असहाय महसूस करती हूं.”
बहार कहती हैं, दशकों से यहां ऐसा ही चल रहा है; पिछले 40 साल से अधिक समय से वह इस गांव में रह रही हैं और यहां कुछ भी नहीं बदला है. समय से पहले जन्म लेने के कारण उनके सात बच्चों की मौत हो गई थी. इसके बाद जो छह बच्चे पैदा हुए वे सभी जीवित हैं. वह बताती हैं, “उस समय यहां कोई अस्पताल नहीं था और आज भी हमारे गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है.”
पारी और काउंटरमीडिया ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण भारत की किशोरियों तथा युवा औरतों को केंद्र में रखकर की जाने वाली रिपोर्टिंग का यह राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट, 'पापुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया' द्वारा समर्थित पहल का हिस्सा है, ताकि आम लोगों की बातों और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए इन महत्वपूर्ण, लेकिन हाशिए पर पड़े समुदायों की स्थिति का पता लगाया जा सके.
इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें
अनुवादः मोहम्मद क़मर तबरेज़