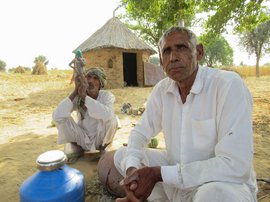यह स्टोरी जलवायु परिवर्तन पर आधारित पारी की उस शृंखला का हिस्सा है जिसने पर्यावरण रिपोर्टिंग की श्रेणी में साल 2019 का रामनाथ गोयनका अवॉर्ड जीता है.
केरल के पहाड़ी वायनाड ज़िले में खेती की अपनी मुश्किलों के बारे में ऑगस्टाइन वडकिल कहते हैं “शाम को 4 बजे हमें यहां गर्म रहने के लिए आग जलानी पड़ती थी. लेकिन यह 30 साल पहले होता था. अब वायनाड में ठंड नहीं है, किसी ज़माने में यहां धुंध हुआ करती थी.” मार्च की शुरुआत में अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस से, अब यहां तापमान वर्ष के इस समय तक आसानी से 30 डिग्री को पार कर जाता है.
और वडकिल के जीवनकाल में गर्म दिनों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर एक इंटरैक्टिव उपकरण से की गई गणना के अनुसार, 1960 में, जिस वर्ष उनका जन्म हुआ था, "वायनाड क्षेत्र में साल के लगभग 29 दिन कम से कम 32 डिग्री [सेल्सियस] तक तापमान पहुंच जाता था." इस गणना को न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इस साल जुलाई में ऑनलाइन पोस्ट किया गया था. गणना के मुताबिक़, “आज वायनाड क्षेत्र में 59 दिन ऐसे होते हैं जब तापमान औसतन 32 डिग्री या उससे ऊपर चला जाता है.”
वडकिल कहते हैं कि मौसम के पैटर्न में बदलाव से गर्मी न झेल पाने वाली फ़सलों, जैसे कि काली मिर्च और संतरे के पेड़ों को नुक़्सान पहुंच रहा है, जो कभी इस ज़िले में डेक्कन पठार के दक्षिणी सिरे पर पश्चिमी घाट में प्रचुर मात्रा में होते थे.
वडकिल और उनकी पत्नी वलसा के पास मनंथवाडी तालुका के चेरुकोट्टुर गांव में चार एकड़ खेत हैं. उनका परिवार लगभग 80 साल पहले कोट्टयम से वायनाड आ गया था, ताकि यहां नक़दी फ़सल की बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपनी क़िस्मत आज़मा सके. वह भारी प्रवासन का दौर था, जब राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थित इस ज़िले में मध्य केरल के हज़ारों छोटे और सीमांत किसान आकर बस रहे थे.
लेकिन समय के साथ, लगता है कि वह तेज़ी मंदी में बदल गई. वडकिल कहते हैं, "बारिश पिछले साल की तरह ही अनियमित रही, तो हम जिस [ऑर्गैनिक रोबस्टा] कॉफ़ी को उगाते हैं, वह बर्बाद हो जाएगी." वलसा कहती हैं, "कॉफ़ी लाभदायक फ़सल है, लेकिन मौसम इसके विकास में सबसे बड़ी समस्या है. गर्मी और अनियमित वर्षा इसे बर्बाद कर देती है." इस सेक्टर में काम करने वाले लोग बताते हैं कि [रोबस्टा] कॉफ़ी उगाने के लिए आदर्श तापमान 23-28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है.

ऊपर की पंक्ति: वायनाड में कॉफ़ी की फ़सल को फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में अपनी पहली बारिश की आवश्यकता होती है और इसके एक सप्ताह बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है. नीचे की पंक्ति: लंबे समय तक सूखा या बेमौसम की बारिश, रोबस्टा कॉफ़ी के बीजों (दाएं) का उत्पादन करने वाले फूलों (बाएं) को नष्ट कर सकती है
वायनाड की सभी कॉफ़ी, जो रोबस्टा परिवार (एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी) में शामिल है, की खेती दिसंबर से मार्च के अंत तक की जाती है. कॉफ़ी के पौधों को फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में पहली बारिश की आवश्यकता होती है - और ये एक सप्ताह बाद फूल देना शुरू कर देते हैं. यह ज़रूरी है कि पहली बौछार के बाद एक सप्ताह तक बारिश न हो, क्योंकि दोबारा बारिश नाज़ुक फूलों को नष्ट कर देती है. कॉफ़ी के फल या ‘चेरी’ को बढ़ना शुरू करने के लिए, पहली बारिश के एक सप्ताह बाद दूसरी बारिश की ज़रूरत होती है. फूल जब पूरी तरह खिलने के बाद पेड़ से गिर जाते हैं, तो फलियों वाली चेरी पकने लगती है.
वडकिल कहते हैं, “समय पर बारिश आपको 85 प्रतिशत उपज की गारंटी देती है." जब हम मार्च की शुरुआत में मिले थे, तो वह ऐसे नतीजे की ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चिंतित थे कि ऐसा होगा भी या नहीं. और अंततः ऐसा नहीं हुआ.
मार्च के आरंभ में, केरल में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ तापमान पहले ही 37 डिग्री पहुंच चुका था. वडकिल ने हमें मार्च के अंत में बताया, “दूसरी बारिश (रंदमथ माझा) इस साल बहुत जल्द आ गई और सबकुछ नष्ट हो गया."
दो एकड़ में इस फ़सल को लगाने वाले वडकिल को इस वजह से इस साल 70,000 रुपए का नुक़्सान हुआ. स्थानीय किसानों से कॉफ़ी ख़रीदने वाली सहकारी समिति, वायनाड सोशल सर्विस सोसायटी (डब्ल्यूएसएसएस), किसानों को एक किलो अपरिष्कृत ऑर्गेनिक कॉफ़ी के 88 रुपए, जबकि नॉन-ऑर्गेनिक कॉफ़ी के 65 रुपए देती है.
डब्ल्यूएसएसएस के निदेशक फ़ादर जॉन चुरापुझायिल ने मुझे फोन पर बताया कि वायनाड में 2017-2018 में कॉफ़ी के 55,525 टन के उत्पादन में इस साल 40 प्रतिशत की गिरावट आई है. अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. फ़ादर जॉन कहते हैं, “उत्पादन में बहुत हद तक यह गिरावट इसलिए आई है, क्योंकि जलवायु में बदलाव वायनाड में कॉफ़ी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हुए हैं." पूरे ज़िले में जिन किसानों से हम मिले वे अलग-अलग वर्षों में अतिरिक्त वर्षा और कभी-कभी कम वर्षा, दोनों से पैदावार में भिन्नता की बात कर रहे थे.


ऑगस्टिन वडकिल और उनकी पत्नी वलसा (बाएं) कॉफ़ी के साथ-साथ रबर , काली मिर्च, केले, धान, और सुपारी भी उगाते हैं. बढ़ती हुई गर्मी ने हालांकि कॉफ़ी (दाएं) और अन्य सभी फ़सलों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है
कम-ज़्यादा बारिश की अनियमितता से खेतों का पानी सूख जाता है. फ़ॉदर जॉन का अनुमान है कि “वायनाड के केवल 10 प्रतिशत किसान ही बोरवेल और पंप जैसी सिंचाई सुविधाओं के साथ सूखे या अनियमित वर्षा के दौरान काम कर सकते हैं.”
वडकिल भाग्यशाली लोगों में से नहीं हैं. अगस्त 2018 में वायनाड और केरल के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ के दौरान उनका सिंचाई पंप क्षतिग्रस्त हो गया था. इसकी मरम्मत कराने पर उन्हें 15,000 रुपए ख़र्च करने पड़ते, जोकि ऐसे मुश्किल समय में बहुत बड़ी राशि है.
अपनी शेष दो एकड़ ज़मीन पर वडकिल और वलसा रबर, काली मिर्च, केले, धान, और सुपारी उगाते हैं. हालांकि, बढ़ती गर्मी ने इन सभी फ़सलों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. “पंद्रह साल पहले, काली मिर्च ही हम सभी को जीवित रखने का स्रोत थी. लेकिन [तब से] ध्रुथवात्तम [तेज़ी से कुम्हलाने] जैसी बीमारियों ने ज़िले भर में इसे नष्ट कर दिया है.” चूंकि काली मिर्च एक बारहमासी फ़सल है, इसलिए किसानों का नुक़्सान विनाशकारी रहा है.
वडकिल कहते हैं, "समय बीतने के साथ, ऐसा लगता है कि खेती करने का एकमात्र कारण यह है कि आपको इसका शौक हो. मेरे पास इतनी सारी ज़मीन है, लेकिन मेरी स्थिति देखें." वह हंसते हुए कहते हैं, "इन मुश्किल घड़ियों में आप केवल इतना कर सकते हैं कि कुछ अतिरिक्त मिर्च पीसें, क्योंकि आप चावल के साथ सिर्फ़ इसे ही खा सकते हैं."
वह कहते हैं, "यह 15 साल पहले शुरू हुआ. कलावस्था इस तरह क्यों बदल रही है?” दिलचस्प बात यह है कि मलयालम शब्द कलावस्था का अर्थ जलवायु होता है, तापमान या मौसम नहीं. यह सवाल हमसे वायनाड के किसानों ने कई बार पूछा था.
बदकिस्मती से, इसका एक जवाब किसानों द्वारा दशकों से अपनाए गए, खेती के तौर-तरीक़ों में निहित है.


अन्य बड़ी भूसंपत्तियों की तरह, मानंथवाडी में स्थित यह कॉफ़ी एस्टेट (बाएं) बारिश कम होने पर कृत्रिम तालाब खोदने और पंप लगाने का ख़र्च उठा सकता है. लेकिन, वडकिल के खेत जैसे छोटे खेतों (दाएं) को पूरी तरह से बारिश या अपर्याप्त कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है
सुमा टीआर कहती हैं, हम कहते हैं कि हर एक भूखंड पर कई फ़सलों को उगाना अच्छा है, बजाय इसके कि एक ही फ़सल लगाई जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है." सुमा, वायनाड के एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन में एक वैज्ञानिक हैं, जो भूमि-उपयोग-परिवर्तन के मुद्दों पर 10 वर्षों तक काम कर चुकी हैं. एक-फ़सली खेती, कीटों और बीमारियों के प्रसार को बढ़ाती है, जिसका इलाज रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों से किया जाता है. ये भूजल में चले जाते हैं या हवा में घुल जाते हैं, जिससे मैलापन और प्रदूषण होता है - और समय के साथ गंभीर पर्यावरणीय क्षति होती है.
सुमा कहती हैं कि यह सब अंग्रेज़ों द्वारा वनों की कटाई से शुरू हुआ. “उन्होंने लकड़ी के लिए जंगलों को साफ़ किया और तमाम ऊंचे पहाड़ों को वृक्षारोपण में बदल दिया.” वह आगे कहती हैं कि जलवायु में परिवर्तन भी इससे जुड़ा हुआ है कि “कैसे [1940 के दशक की शुरुआत से ही ज़िले में] बड़े पैमाने पर प्रवासन के साथ हमारा परिदृश्य भी बदल गया. इससे पहले, वायनाड के किसान मुख्य रूप से अलग-अलग फ़सलों की खेती किया करते थे.”
उन दशकों में, यहां की प्रमुख फ़सल धान थी, कॉफ़ी या काली मिर्च नहीं - ख़ुद ‘वायनाड’ शब्द भी ‘वायल नाडु’ या धान के खेतों की भूमि से आता है. वे खेत इस क्षेत्र - और केरल के पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण थे. लेकिन धान का रकबा (1960 में लगभग 40,000 हेक्टेयर था) आज बमुश्किल 8,000 हेक्टेयर रह गया है; जोकि 2017-18 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ज़िले के सकल फ़सली क्षेत्र के 5 प्रतिशत से भी कम है. और अब वायनाड में कॉफ़ी बाग़ान लगभग 68,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं, जोकि केरल में कुल कॉफ़ी क्षेत्र का 79 प्रतिशत हैं - और 1960 में देश भर में सभी रोबस्टा से 36 प्रतिशत अधिक था, वडकिल का जन्म उसी साल हुआ था.
सुमा कहती हैं, "किसान नक़दी फ़सलों के लिए ज़मीन साफ़ करने के बजाय, पहाड़ी पर रागी जैसी फ़सलों की खेती कर रहे थे." खेत, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सक्षम थे. लेकिन, वह आगे जोड़ती हैं कि बढ़ते पलायन के साथ नक़दी फ़सलों ने खाद्य फ़सलों पर बढ़त बना ली. और 1990 के दशक में वैश्वीकरण के आगमन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने काली मिर्च जैसे नक़दी फ़सलों पर पूरी तरह से निर्भर होना शुरू कर दिया.
पूरे ज़िले में हम जितने भी किसानों से मिले उन सभी ने इस गंभीर परिवर्तन की बात कही - 'उत्पादन में गिरावट इसलिए आई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वायनाड में कॉफ़ी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हुआ है’
डब्ल्यूएसएसएस के एक पूर्व परियोजना अधिकारी, और मानंथवाडी शहर के एक ऑर्गेनिक किसान, ईजे जोस कहते हैं, "आज, किसान एक किलोग्राम धान से 12 रुपए और कॉफ़ी से 67 रुपए कमा रहे हैं. हालांकि, काली मिर्च से उन्हें प्रति किलो 360 रुपए से 365 रुपए मिलता है." मूल्य में इतने बड़े अंतर ने कई और किसानों को धान की खेती छोड़, काली मिर्च या कॉफ़ी का विकल्प चुनने पर मजबूर किया. “अब हर कोई वही उगा रहा है जो सबसे ज़्यादा लाभदायक हो, न कि जिसकी ज़रूरत है. हम धान भी खो रहे हैं, जोकि एक ऐसी फ़सल है जो बारिश होने पर पानी को अवशोषित करने में मदद करती है, और पानी की तालिकाओं को पुनर्स्थापित करती है.”
राज्य में धान के तमाम खेतों को भी प्रमुख रियल एस्टेट भूखंडों में बदल दिया गया है, जो इस फ़सल की खेती में कुशलता रखने वाले किसानों के कार्यदिवस को घटा रहा है.
सुमा कहती हैं, "इन सभी परिवर्तनों का वायनाड के परिदृश्य पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है. एक फ़सली खेती के माध्यम से मिट्टी को बर्बाद किया गया है. बढ़ती हुई जनसंख्या [1931 की जनगणना के समय जहां 100,000 से कम थी, वहीं 2011 की जनगणना के समय 817,420 तक पहुंच गई] और भूमि विखंडन भी इसके साथ जारी है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वायनाड का मौसम गर्म होता जा रहा है.”
जोस भी यह मानते हैं कि कृषि के इन बदलते तरीक़ों का तापमान की वृद्धि से क़रीबी रिश्ता है. वह कहते हैं, “कृषि के तरीक़ों में बदलाव ने वर्षा में परिवर्तन को प्रभावित किया है."
पास की थविनहल पंचायत में, अपने 12 एकड़ के खेत में हमारे साथ घूमते हुए, 70 वर्षीय एमजे जॉर्ज कहते हैं, “ये खेत किसी ज़माने में काली मिर्च से इतने भरे होते थे कि सूरज की किरणों का पेड़ों से होकर गुज़रना मुश्किल होता था. पिछले कुछ वर्षों में हमने कई टन काली मिर्च खो दी है. जलवायु की बदलती परिस्थितियों के कारण पौधों के तेज़ी से मुर्झाने जैसी बीमारियां हो रही हैं.”
फंगस फ़ाइटोफ्थोरा के कारण, तेज़ी से मुर्झाने की समस्या ने ज़िले भर के हज़ारों लोगों की आजीविका को समाप्त कर दिया है. जोस कहते हैं, "यह उच्च आर्द्रता की स्थितियों में पनपता है, और इसमें पिछले 10 वर्षों में वायनाड में काफ़ी वृद्धि हुई है. बारिश अब अनियमित होती है. रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने भी इस रोग को फैलने में मदद की है, जिससे ट्राइकोडर्मा नामक अच्छे बैक्टीरिया धीरे-धीरे मरने लगते हैं, जो फंगस से लड़ने में मदद करता था.”

सबसे ऊपर बाएं: एमजे जॉर्ज कहते हैं, ‘हम अपनी वर्षा के लिए प्रसिद्ध थे’. सबसे ऊपर दाएं: सुभद्रा बालकृष्णन कहती हैं, 'इस साल हमें कॉफ़ी की सबसे कम पैदावार मिली.' सबसे नीचे बाएं: वैज्ञानिक सुमा टीआर कहती हैं कि यह सब अंग्रेज़ों द्वारा वनों की कटाई के बाद शुरू हुआ. सबसे नीचे दाएं: ईजे जोस कहते हैं, ‘आजकल हर कोई वही उगा रहा है जो सबसे ज़्यादा लाभदायक हो, न कि वह जिसकी ज़रूरत है'
जॉर्ज कहते हैं, “पहले हमारे पास वायनाड में वातानुकूलित जलवायु थी, लेकिन अब नहीं है. बारिश, जो पहले वर्षा ऋतु में लगातार होती थी, अब पिछले 15 वर्षों के दौरान इसमें काफ़ी कमी आई है. हम अपनी वर्षा के लिए प्रसिद्ध थे…”
भारत मौसम विज्ञान विभाग (तिरुवनंतपुरम) का कहना है कि 2019 में 1 जून से 28 जुलाई के बीच वायनाड में सामान्य औसत से 54 प्रतिशत कम बारिश हुई थी.
आम तौर पर उच्च वर्षा का क्षेत्र होने की वजह से, वायनाड के कुछ हिस्सों में कई बार 4,000 मिमी से अधिक बारिश होती है. लेकिन कुछ वर्षों से बारिश के मामले में ज़िले के औसत में बेतहाशा उतार-चढ़ाव हुआ है. 2014 में आंकड़ा 3,260 मिमी था, लेकिन उसके बाद अगले दो वर्षों में भारी गिरावट के साथ यह 2,283 मिमी और 1,328 मिमी पर पहुंच गया. फिर, 2017 में यह 2,125 मिमी था और 2018 में, जब केरल में बाढ़ आई थी, यह 3,832 मिमी की ऊंचाई पर पहुंच गया.
केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर की जलवायु परिवर्तन शिक्षा और अनुसंधान अकादमी में वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत डॉ गोपाकुमार चोलायिल कहते हैं, "हाल के दशकों में वर्षा की अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता में बदलाव हुआ है, विशिष्ट रूप से 1980 के दशक से; और 90 के दशक में इसमें तेज़ी आई. साथ ही, मानसून तथा मानसून के बाद की अवधि में पूरे केरल में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ी हैं. वायनाड इस मामले में कोई अपवाद नहीं है.”
यह सब वास्तव में, वडकिल, जॉर्ज, तथा अन्य किसानों की चिंताओं की पुष्टि करता है. भले ही वे बारिश की ‘कमी’ का शोक मना रहे हैं - और ज़िले की दीर्घकालिक औसत भी गिरावट का संकेत दे रहे हैं - लेकिन उनके कहने का मतलब यही है कि जिन मौसमों और दिनों में उन्हें बारिश की ज़रूरत और उम्मीद होती है उनमें वर्षा बहुत कम होती है. यह ज़्यादा वर्षा के साथ-साथ, कम बारिश के वर्षों में भी हो सकता है. जितने दिनों तक बारिश का मौसम रहता था अब उन दिनों में भी कमी आ गई है, जबकि इसकी तीव्रता बढ़ गई है. वायनाड में अभी भी अगस्त-सितंबर में बारिश हो सकती है, हालांकि, यहां मानसून का मुख्य महीना जुलाई है. (और 29 जुलाई को, मौसम विभाग ने इस ज़िले के साथ-साथ कई अन्य ज़िलों में ‘भारी’ से ‘बहुत भारी’ बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया था.)


वायनाड में वडकिल के नारियल तथा केले के बाग़ान, अनिश्चित मौसम के कारण धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं
डॉ. चोलायिल कहते हैं, "फ़सल के तौर-तरीक़ों में बदलाव, जंगल की कटाई, भूमि उपयोग के अलग-अलग रूप...इन सबका पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर असर पड़ा है."
सुभद्रा (जिन्हें मनंथवाडी में लोग प्यार से ‘टीचर’ कहके पुकारते हैं) कहती हैं, "पिछले साल की बाढ़ में मेरी कॉफ़ी की पूरी फ़सल नष्ट हो गई थी. " यह 75 वर्षीय किसान (सुभद्रा बालकृष्णन) आगे जोड़ती हैं, “इस साल वायनाड में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे कम हुआ.” वह एडवाक पंचायत में अपने परिवार की 24 एकड़ ज़मीन पर खेती की निगरानी करती हैं और अन्य फ़सलों के अलावा, कॉफ़ी, धान, और नारियल उगाती हैं. उनके मुताबिक़, “वायनाड में [कॉफ़ी के] कई किसान [आय के लिए] अब पहले से ज़्यादा अपने मवेशियों पर निर्भर होते जा रहे हैं.”
हो सकता है कि वे ‘जलवायु परिवर्तन’ शब्द का उपयोग न करते हों, लेकिन हम जितने भी किसानों से मिले वे सभी इसके प्रभावों से चिंतित हैं.
अपने अंतिम पड़ाव पर - सुल्तान बाथेरी तालुका की पूथडी पंचायत में 80 एकड़ में फैली एडेन घाटी में – हम पिछले 40 वर्षों से खेतिहर मज़दूरी कर रहे गिरीजन गोपी से मिले; जब वह अपना आधा ख़त्म ही करने वाले थे. उन्होंने कहा, “रात में बहुत ठंड होती है और दिन में बहुत गर्मी. कौन जानता है कि यहां क्या हो रहा है." अपने दोपहर के भोजन के लिए जाने से पहले उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा (या शायद ख़ुद से कहा): “यह सब भगवान की लीला है. वरना इन सब बातों की कोई कैसे समझे?"
कवर फ़ोटो: विशाखा जॉर्ज
लेखिका, इस स्टोरी को पूरा करने में मदद के लिए शोधकर्ता नोएल बेनो को धन्यवाद देती हैं.
पारी का जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट, यूएनडीपी समर्थित उस पहल का एक हिस्सा है जिसके तहत आम अवाम और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को दर्ज किया जाता है.
इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] को लिखें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें
अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़
#deforestation #quick-wilt #rising-temperature #wayanad #erratic-rainfall #changes-in-cropping-patterns #pepper #robusta-coffee